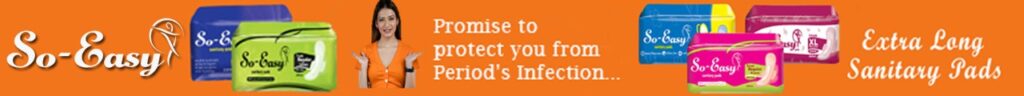वी.एस. नायपॉल सच को पूरी बेबाकी से बयान करने वाले रचनाकार थे। दुनिया के बारे में हो या अपने बारे में, लिखते हुए उन्होंने सच्चाई को सबसे ऊपर रखा। अपने पुरखों की भूमि भारत के बारे में भी उन्होंने इसी निर्मम ममता के साथ कलम चलाई। वे भारतीयों को अपने ही देश को कुछ हटकर देखना सिखा गए…आगे बढ़ें प्रो हरीश त्रिवेदी की नजर में वी.एस.नायपॉल कैसे थे-
वी.एस. नायपॉल जितने महान लेखक थे उतने ही खरे व ईमानदार व्यक्ति। वे सच बोलने से कभी नहीं हिचके, न दुनिया-जहान के बारे में और न ही खुद अपने बारे में। वे ‘सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात’ की ढकोसले वाली नीति से कोसों दूर रहे, वे तो ‘सत्यमेव जयते’ के उपासक थे। उनकी दृष्टि जितनी पैनी है उनका गद्य उतना ही पारदर्शी, तो उनका लिखा कुछ भी पढ़कर सहज ही विश्वास जागता है कि यही सच है। चाहे व्यक्ति और समाज की विसंगतियां दर्शाते उनके उपन्यास हों, चाहे उनके विश्वव्यापी यात्रावृत्त जिनमें चिंतन और सभ्यता-समीक्षा का स्वर प्रमुख है, उनकी सभी पुस्तकों में हमारे उत्तर-औपनिवेशिक जगत का पूरा कच्चा-चिट्ठा दर्ज है। .
उनसे पहली बार मेरा मिलना हुआ 1998 में, ठीक 20 साल पहले। उनकी एक पुस्तक का विमोचन था यहीं दिल्ली के एक बड़े होटल में। मै पहुंचा तो पेंग्विन इंडिया के मुख्य अधिकारी डेविड देवीदार मुझे सीधे नायपॉल से मिलाने ले गए और उनसे हाथ मिलाते ही मैंने कहा, ‘आपकी पुस्तकें मुझे जितनी अच्छी लगती हैं उतनी किसी और समकालीन लेखक की नहीं।’ .
यह सुन कर न वे मुस्कराए और न उन्होंने ‘थैंक यू’ कहने की औपचारिकता निभाई। मेरी ओर गौर से देखा और बोले, ‘वैसे आपने पढ़ा क्या है?’ मुझे मजा आ गया। यही तो हैं वे बेबाक-बेलाग नायपॉल जिनका मैं मुरीद हूं! मैंने एक-ही सांस में उनकी सभी पुस्तकों के नाम सिलसिलेवार गिनाने शुरू किए, प्रकाशन के काल-क्रम से। (मैं कई वर्षों से न केवल नायपॉल को पढ़ रहा था बल्कि उनका एक उपन्यास दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा भी रहा था।) अब वे मुस्कराए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे रोका, और बोले, ‘माफ़ कीजिए, अभी दो मिनट पहले एक महिला आई थीं, उन्होंने भी मेरी तारीफ की और मैंने पूछा कि आपने पढ़ा क्या है तो एक भी पुस्तक का नाम नहीं ले पाईं।’ फिर हम लोगों की जमकर बातचीत हुई, उन्होंने मुझे अपना इंग्लैंड का फोन और पता दिया, और वहां लौटकर तुरंत पत्र लिखा। .
नायपॉल की प्रसिद्धि हुई उनके चौथे उपन्यास ‘ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास’ (1961) से, जिसका परिदृश्य त्रिनिदाद का है। नायपॉल के पूर्वज गोरखपुर जिले के एक गांव से चल कर गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत आधी दुनिया पार त्रिनिदाद में गन्ने के खेतों में मजूरी करवाने के लिए ले जाए गए थे, फिर धीरे-धीरे पढ़ लिखकर शहर तक पहुंचे। इस उपन्यास का मुख्य चरित्र नायपॉल के पिता पर आधारित है जो पत्रकार थे और उपन्यासकार होना चाहते थे, नायपॉल का स्वयं भी किशोरावस्था का मार्मिक आत्म-चित्रण है, और एक ही घर में साथ रहने वाले भरे-पूरे संयुक्त परिवार के उलझते-सुलझते रिश्तों की इतनी सजीव तस्वीर कि हिंदी साहित्य में भी शायद ढूंढ़े न मिले। मुख्य स्वर विनोदात्मक है जिसमें पात्रों की अनेक असफलताओं और असमर्थताओं के प्रति सहानुभूति का भाव है, व्यंग्य का नहीं। .
नायपॉल के स्वर में तल्खी तो बाद में आई जब उन्होंने दुनिया देखी और पाया कि उपनिवेशवादी शक्तियों ने इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक जहां-जहां राज किया वहां मनुष्य को और समाज को आधा-अधूरा ही नहीं बल्कि अपना नकलची बना कर छोड़ दिया, उसकी स्वाभाविकता और मूल प्रकृति ही हर ली। उनका एक उपन्यास है ‘द मिमिक मेन’ (1967; नकलची लोग) जिसमें उन्होंने दिखलाया है कि शासित व्यक्ति की विडंबना यही है कि वह स्वतंत्र होकर भी बस शासक जैसा ही बन जाना चाहता है। .
अब तक नायपॉल खुद त्रिनिदाद छोड़ कर इंग्लैंड आ गए थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़कर बीबीसी में नौकरी करने लगे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहां के हैं और अब कहां रहें। तभी वे सालभर के लिए भारत आए, अपनी जड़ें तलाशते और यह भी सूंघते कि तीन पीढ़ी बाद ही सही, प्रवास समाप्त कर फिर भारत में रहा जा सकता है क्या? वे लंदन से ही भारत में कम-से-कम तीन नौकरियों के लिए आवेदन दे चुके थे और अब खुद आकर देखना चाहते थे कि क्या संभावना है। .
पर भारत आते ही वे यहां की हर-एक बात से क्षुब्ध और विचलित हुए। उस यात्रा के बाद लिखी पुस्तक ‘एन एरिया ऑफ डार्कनेस’ (1964 : अंधकार का दायरा) में उन्होंने यहां की दारुण गरीबी, संपन्न लोगों द्वारा उसे सर्वथा अनदेखा करना, दिशा-मैदान जाने की प्रवृत्ति, नौकरशाही की धौंस, विदेशी चीजों के प्रति अंध-मोह आदि अनेक बातों का ऐसा तीखा वर्णन किया कि उस पुस्तक का हमारे अंग्रेजीदां पाठकों पर कुछ वैसा ही प्रभाव पड़ा जैसा कि चार-साल बाद छपे श्रीलाल शुक्ल के ‘राग दरबारी’ का हिंदी समाज पर। जैसा हम सब का आजादी के सपनों से मोहभंग हुआ कुछ वैसा ही नायपॉल का भारत से। .
पर जब 2001 में नायपॉल को नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि त्रिनिदाद का नहीं उन दो देशों का नाम लिया जहां से वे अपने को जुड़ा हुआ मानते रहे, इंग्लैंड जहां वे रहते आए थे और भारत जो उनसे छोड़े नहीं छूटा। भारत पर उनकी निर्मम ममता सदैव बनी रही और हमें भी अपने ही देश को कुछ हटकर देखना सिखा गई।